सामाजीकरण की अवधारणाएँ
समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। समाजीकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखण्ड तथा सतत रहता है, बल्कि इसी से मानवोचित गुणों का विकास भी होता है और व्यक्ति सुसभ्य व सुसंस्कृत भी बनता है। संस्कृति का हस्तान्तरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के बिना व्यक्ति सामाजिक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अत: यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है, जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। इस तरह यह सांस्कृतिक मूल्यों, प्राथमिकताओं और प्रतिमानों को बच्चों के व्यवहार में संक्रमित करने की प्रक्रिया है। यह विभिन्न प्रक्रियाओं, शैक्षिक संस्थाओं और लोगों द्वारा सम्पन्न होती है।
समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यावहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना, आता है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता, माता-पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएँ और जनसंचार माध्यम जैसे-दूरदर्शन इत्यादि। वे प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को पालने की प्रक्रिया में प्रभाव डालते हैं साथ-ही-साथ अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक उचित तरीके के विचार और व्यवहार को बल देते हैं। प्रारम्भिक बाल्यकाल विकास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इस समय बच्चे अपने परिवारों, समाज और संस्कृति के रीति-रिवाज और रीतियों के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे भाषा ग्रहण करते हैं और संस्कृति के आधारभूत सिद्धान्त सीखते हैं। इस अवस्था में प्राथमिक समाजीकरण के अभिकर्ता परिवार के सदस्य होते हैं। मध्य बाल्यकाल में परिवार महत्वपूर्ण होते हुए भी समवयस्कों एवं विद्यालय का प्रभाव प्रमुख हो जाता है। संचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन और कम्प्यूटर का प्रभाव अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
यही वह समय है जब सामाजिक रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह विकसित होने की अधिक सम्भावना होती है। कई शोध किए गए हैं कि पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। परिवार, साथी, संचार माध्यम और विद्यालय के अतिरिक्त भी कुछ दूसरे कारक हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। माता-पिता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और कुल परम्परा बच्चों के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं। कुल परम्परा (एथनीसिटी) परिवार के आकार, संरचना, शिक्षा, आय, रचना और फैले हुए जाल से जुड़ी होती है।
शैक्षिक समाजशास्त्र के विद्वान् बोगार्डस ने समाजीकरण की परिभाषा इस प्रकार दी है 'समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक कल्याण हेतु एक-दूसरे पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखते हैं और जिसके द्वारा सामाजिक आत्म-नियन्त्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सन्तुलित व्यक्तित्व का अनुभव प्राप्त करते हैं"।
समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही सम्भव है, समाज से अलग रहकर नहीं। यह व्यक्ति को सामाजिक परम्पराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदशाँ आदि का पालन करना और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाता है। समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता और अन्य अनगिनत विशेषताएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होती हैं और जीवित रहती हैं।
समाजीकरण के कारक
किसी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया के महत्वपर्ण कारक निम्न प्रकार से है।
पालन पोषण
बालक के समाजीकरण पर पालन-पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारम्भिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता-पिता बालक का पालन-पोषण करते हैं उसी के अनुसार बालक में भावनाएँ तथा अनुभूतियाँ विकसित हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस बालक की देख-रेख उचित ढंग से नहीं होती उसमें समाज विरोधी आचरण विकसित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह अपने को समाज के साथ व्यवस्थापित नहीं कर पाता। इस दृष्टि से उचित समाजीकरण के लिए यह आवश्यक है कि बालक का पालन-पोषण ठीक प्रकार से किया जाए।
सहानुभूति
पालन-पोषण की भाँति सहानुभूति का भी बालक के समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि शैशवावस्था में बालक अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहता है। दूसरे शब्दों में, अन्य व्यक्तियों द्वारा बालक की आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि बालक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना ही सब कुछ नहीं है वरन् उसके साथ सहानुभूति रखना भी आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणामस्वरूप वह एक-दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है, जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है।
सहकारिता
व्यक्ति को समाज ही सामाजिक बनाता है। दूसरे शब्दों में, समाज की सहकारिता बालक को सामाजिक बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे-जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता जाता है, वैसे-वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरम्भ कर देता है। इससे उसकी सामाजिक प्रवृत्तियाँ संगठित हो जाती हैं।
निर्देश
सामाजिक निर्देशों का बालक के समाजीकरण में गहरा हाथ होता है। ध्यान देने की बात यह है कि बालक जिस कार्य को करता है, उसके सम्बन्ध में वह दूसरे व्यक्तियों से निर्देश प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, वह उसी कार्य को करता है, जिसको करने के लिए उसे निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि निर्देश सामाजिक व्यवहार की दिशा को निर्धारित करता है।
आत्मीकरण
माता-पिता, परिवार तथा पड़ोस की सहानुभूति द्वारा बालक में आत्मीकरण की भावना का विकास होता है। जो लोग बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, उन्हीं को बालक अपना समझने लगता है तथा उन्हीं के रहन- सहन, भाषा तथा आदशों के अनुसार व्यवहार करने लगता है।
अनुकरण
समाजीकरण का आधारभूत तत्व अनुकरण है। ध्यान देने की बात यह है कि बालक में अनुकरण का विकास परिवार तथा पड़ोस में रहते हुए होता है। दूसरे शब्दों में, बालक परिवार तथा पड़ोस के लोगों को जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखता है, वह उसी प्रकार का अनुकरण करने लगता है।
सामाजिक शिक्षण
अनुकरण के अतिरिक्त सामाजिक शिक्षण का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का आरम्भ परिवार से होता है जहाँ पर बालक माता-पिता, भाई-बहन तथा अन्य सदस्यों से खान-पान तथा रहन-सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता रहता है।
पुरस्कार एवं दण्ड
बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दण्ड का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के आदशों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही वह समाज के हित की दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है, तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है, तो दण्ड दिया जाता है जिसके भय से वह ऐसा कार्य फिर दोबारा नहीं करता। स्पष्ट है, पुरस्कार एवं दण्ड का बालक के समाजीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
बालकों का समाजीकरण करने वाले तत्व
बालक जन्म के समय कोरा पशु होता है। जैसे-जैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं के सम्पर्क में आकर विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है, वैसे-वैसे वह अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण करते हुए सामाजिक आदशों तथा मूल्यों को सीखता रहता है। इस प्रकार, बालक के समाजीकरण की यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।
बालक के समाजीकरण में उसका परिवार, पड़ोस, स्कूल, उसके साथी, उसका समुदाय, धर्म, इत्यादि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
वंशानुक्रम
बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे- मूलभाव, संवेग, सहज क्रियाएँ व क्षमताएँ आदि। इनके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं।
परिवार
बालक के समाजीकरण के विभिन्न तत्वों में परिवार का प्रमुख स्थान है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी-न-किसी परिवार में ही होता है। जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे-वैसे वह अपने माता-पिता, भाई-बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सम्पर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। यही नहीं, वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शी, मूल्यों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं तथा मान्यताओं एवं विश्वासों को भी धीरे-धीरे सीख जाता है।
पड़ोस
पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार, बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अन्तःक्रिया द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के सम्पर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है, तो उसका बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और यदि पड़ोस खराब है, तो बालक के बिगड़ने की सम्भावना है। यही कारण है कि अच्छे परिवारों के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसन्द करते हैं।
स्कूल
परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है जिससे उसका समाजीकरण तीव्रगति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहाँ एक ओर विभिन्न विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, मान्यताओं, विश्वासों तथा आदशों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है वहीं दूसरी ओर उसमें स्कूल की विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता रहता है। इस दृष्टि से परिवार तथा पड़ोस की भाँति स्कूल भी बालक के समाजीकरण का मुख्य साधन है।
बालक के साथी
प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है। वह खेलते समय जाति-पाँति, ऊँच-नीच तथा अन्य प्रकार के भेद भावों से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अन्तःक्रिया द्वारा आनन्द लेना चाहता है। इस कार्य में उसके साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
समुदाय
बालक के समाजीकरण में समुदाय अथवा समाज का गहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने-अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। इन साधनों के अन्तर्गत जातीय तथा राष्ट्रीय प्रथाएँ एवं परम्पराएँ मनोरंजन एवं पूर्वधारणाएँ इत्यादि आती हैं।
धर्म
धर्म का बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार, परम्पराएँ, आदर्श तथा मूल्य होते हैं। जैसे-जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तित्व एवं समूहों के सम्पर्क में आता जाता है, वैसे-वैसे वह उक्त सभी बातों को स्वाभाविक रूप से सीखता है।
समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका
(1) विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, बल्कि यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है और विद्यालय के इस । कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है।
(2) परिवार के बाद बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिलता है। अध्यापक ही शिक्षा के द्वारा बच्चे में वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है, जो समाज व संस्कृति में मान्य होते हैं।
(3) स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। इस प्रकार, विद्यालय बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धान्तों की नींव डालता है।
(4) समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता-पिता से सम्पर्क स्थापित करके उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे एवं उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने के अवसर प्रदान करे।
(5) शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करे। इन क्रियाओं में भाग लेने से उसका समाजीकरण स्वत: हो जाएगा।
(6) बालक के समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय सम्बन्धों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अत: शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बालकों, शिक्षकों तथा स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ स्वस्थ मानवीय सम्बन्ध स्थापित करे। इन स्वस्थ मानवीय सम्बन्धों के स्थापित हो जाने से स्कूल का समस्त वातावरण सामाजिक बन जाएगा
(7) बच्चे को सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों आदि का ज्ञान देना उनके समाजीकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। जहाँ तक सामाजिक भूमिका की प्रत्याशा एवं उनके निर्वाह का प्रश्न है, तो अध्यापक स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें अनुकरण हेतु प्रेरित कर सकता है।
(8) विद्यार्थियों से घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें अपनी अभिवृत्तियों की समीक्षा करने हेतु प्रोत्साहित कर तथा उनकी वर्तमान अभिवृत्तियों का समर्थन कर उनके समाजीकरण में सहायता की जा सकती है। समाजीकरण के मामले में बच्चे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं।
बच्चे के समाजीकरण में परिवार एवं माता-पिता की भूमिका
समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार व माता-पिता का असाधारण महत्व है। यह कहा जाता है कि माँ के त्याग और पिता की सुरक्षा में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है, वह उसके जीवन की स्थायी पूँजी होती है। बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेकर परिवार का सदस्य बनता है। उसका सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध अपनी माँ से होता है। माँ उसे दूध पिलाती है और तरह-तरह से उसकी रक्षा करती है।
बच्चे को नियमित रूप से खाने-पीने की, पहनने की तथा रहने की सीख उसे माँ से मिलती है। इससे बच्चे के मन में एक सुरक्षा की भावना पनपती है जो उसके जीवन को स्थिर तथा दृढ़ बनाती है और आगे चलकर उसे उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता देती है। माता और पिता से बच्चे की अधिकतर आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। साथ ही बच्चा यह देखता है कि कुछ कार्यों को करने पर माता या पिता उसे प्यार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और कुछ कार्यों के करने से उसे दण्ड मिलता है व उसकी निन्दा होती है। परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि उसे कौन-कौन से काम करने चाहिएँ और किन-किन कार्यों से बचना चाहिए? इससे बच्चा धीरे-धीरे यह सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा और समाज उससे क्या चाहता है? जो समाज में प्रचलित होते हैं तथा समाज को मान्य होते हैं।
माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं। वे उसके साथ हँसते-बोलते हैं। बच्चा उनकी ओर देखता है, उनके होंठों को हिलाकर बातें करने की प्रक्रिया को बार-बार देखता और फिर उसी की नकल उतारने का प्रयास करता है। इसी के परिणामस्वरूप समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण पक्ष भाषा का विकास उसमें होता है। परिवार में प्राय: एक से अधिक सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक के अलग-अलग मिजाज, रुचि, व्यवहार के तरीके, भावनाएँ आदि होती हैं फिर भी इनमें से प्रत्येक के साथ बच्चे को घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना होता है, क्योंकि परिवार के एक छोटे-से दायरे के साथ किस प्रकार मिलकर रहा जाता है, दूसरों से किस प्रकार अनुकूलन किया जाता है? इस अनुकूलन के दौरान उसमें सहनशीलता का गुण भी पनप जाता है।
परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं, जो समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण कहते हैं। परिवार में रहकर बच्चा माँ-बाप से सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है तथा अपनी मौलिक धारणाओं, आदर्श एवं शैली की रचना करता है। यदि परिवार में परस्पर सहयोग की भावना हो, तो बालक में भी सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चे की यह भावना उसके बाह्य समाज से व्यवहार में भी झलकती है। माँ-बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार के आर्थिक स्तर का भी बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। सम्पन्न परिवारों के बच्चों में सामान्यत: स्वयं
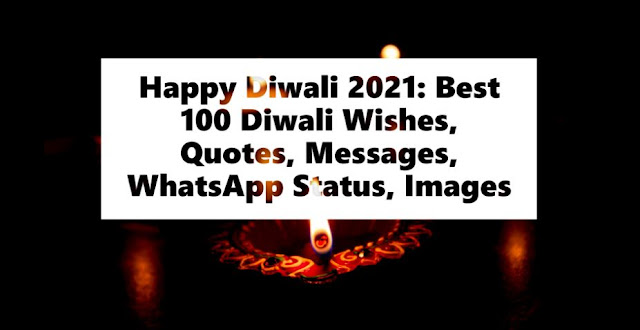
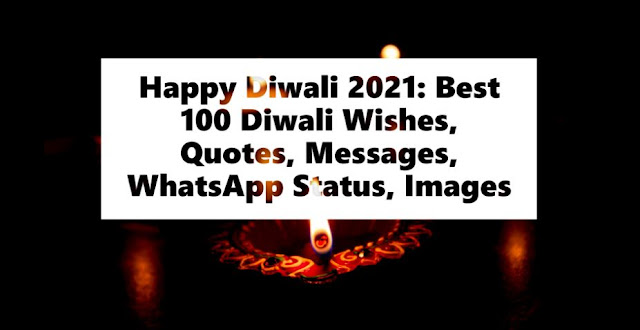
Comments
Post a Comment