5 - पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धान्त
विकास की अवस्थाओं के सिद्धान्त
मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं।
विकास की विभिन्न अवस्था में बालक में विशेष प्रकार के गुण एवं विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। इनका अध्ययन कर कई मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के सन्दर्भ में विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।
विकास की अवस्थाओं से सम्बन्धित सिद्धान्तों में जीन पियाजे, लॉरेन्स कोह्नबर्ग एवं वाइगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त सिद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धान्त
जीन पियाजे स्विट्जरलैण्ड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बचे जैसे-जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास सम्बन्धी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रति दून किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है।
संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएँ एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिन्तन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल हैं।
पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धान्त के अनुसार, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाती है।
पियाजे ने अपने इस सिद्धान्त के अन्तर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने सम्बन्धी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुँचना आदि को लेकर पैदा होता है। अत: जन्म ' के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परन्तु जैसे-जैसे वह बड़ा होता है उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। पियाजे ने बालकों में बुद्धि का इस प्रकार क्रमिक विकास अर्थात् संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनके नाम एवं विशेषताएँ नीचे की सारणी में दी गई हैं-
(1) इन्द्रियजनित गामकं अवस्था (जन्म से 2 वर्ष तक)
मानसिक क्रियाएँ इन्द्रियजनित गामक क्रियाओं के रूप में ही सम्पन्न होती हैं।
भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है।
जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्षत: देखते हैं, उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है।
इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए, चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है।
इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से सम्बन्धित है।
(2) पूर्व संक्रियात्मक अवस्था (2 से 7 वर्ष तक)
इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है।
इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारम्भ हो जाता है।
इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है।
(3) मूर्त संक्रियात्मक अवस्था (7 से 11 वर्ष तक)
इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण
करने की क्षमता विकसित हो जाती है।
उनका चिन्तन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारम्भ कर देता है।
इस अवस्था में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लम्बाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं।
बालक किसी पूर्व और उसके अंश के सम्बन्ध में तर्क कर सकता है।
बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है।
(4) अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था (11 वर्ष से आगे)
यह अवस्था ग्यारह वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है।
अमूर्त चिन्तन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है।
इस अवस्था में भाषा सम्बन्धी योग्यता तथा सम्प्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊँचाई को
छूने लगता है।
बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है।
जीन पियाजे के अन्य सिद्धान्त
निर्माण और खोज का सिद्धान्त
प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार सम्बद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय-समय पर खोज और निर्माण करते हैं, जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है।
पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। नवीनता या खोज को उद्दीपक-अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक चार साल का बालक यदि भिन्न-भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है, तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से सम्बन्धित है।
कार्य-क्रिया का अर्जन
कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है, जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रणशीलता है।
प्रत्येक कार्यात्मक-क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत होता है। उदाहरण के लिए, एक मिट्टी के चक्र को दो भागों में तोड़ना तथा दो टूटे हुए भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्यात्मक-क्रिया है। कार्यात्मक-क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहाँ पुन: पहुँच सकते हैं जहाँ से उन्होंने कार्य प्रारम्भ किया था।
बौद्धिक वृद्धि का केन्द्र इन्हीं कार्यात्मक-क्रिया का अर्जन है।
पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोर अवस्था तक नहीं पहुँच जाता है तब तक वह भिन्न-भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न वर्गों के कार्यात्मक-क्रिया का अर्जन करता रहता है।
एक विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण के लिए दो तथ्य आवश्यक हैं - सात्मीकरण एवं सन्तुलन स्थापित करना।
सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नये विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। पियाजे के अनुसार, सात्मीकरण बालक के प्रत्यक्षात्मक-गत्यात्मक समन्वय से सम्बन्धित है।
व्यवस्थापन या सन्तुलन का अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नये विचारों और वस्तुओं में फिट करना।
लॉरेन्स कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धान्त
बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के सन्दर्भ में लॉरेन्स कोह्नबर्ग ने अपने अनुसन्धानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक स्तर अथवा अवस्थाएँ पाई जाती हैं।
ये अवस्थाएँ या स्तर इस प्रकार हैं ।
पूर्व नैतिक स्तर
परम्परागत नैतिक स्तर
आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर
पूर्व नैतिक अवस्था या स्तर बालक 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, परम्परागत नैतिक अवस्था या स्तर 10 तथा 13 वर्ष के दौरान एवं आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर या अवस्था 13 वर्ष से प्रारम्भ होकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है।
कोहलवर्ग द्वारा प्रदत्त इस प्रकार के वर्गीकरण को कुछ और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए, तो निम्न प्रकार के वर्गीकरण द्वारा बालकों के नैतिक या चारित्रिक विकास की पाँच प्रमुख स्तर या अवस्थाऍ तय की जा सकती है।
पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेन्द्रित अवस्था, परम्पराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था एवं आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था।
पूर्व नैतिक
यह अवस्था जन्म से लेकर दो वर्ष की आयु तक विद्यमान रहती है।
इस अवस्था में बालक से किसी प्रकार की नैतिकता या चारित्रिक मूल्यों को धारण करने की बात ही नहीं उठती है, क्योंकि इस स्तर पर उसे यह समझ नहीं होती कि उसके ऐसा करने से किसी अन्य को नुकसान या परेशानी होगी।
क्या अच्छा है क्या बुरा, यह बात उसकी समझ से बाहर ही होती है। उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं तथा संवेगों पर नियन्त्रण करना नहीं आता और परिणामस्वरूप वह अपनी मर्जी का मालिक बनकर इच्छित व्यवहार करने की जिद पकड़ता रहता है।
कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरण
आत्मकेन्द्रित निर्णय (वैयक्तिकता ओर विनियम)
यान्त्रिक सापेक्षिक उन्मुखीकरण
परस्पर एकरूप उन्मुखीकरण (अच्छे अन्त:वैयक्तिक सम्बन्ध)
अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण
सामाजिक अनुबन्ध एवं व्यक्तिगत अधिकार उन्मुखीकरण
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धान्त उन्मुखीकरण ।
स्वकेन्द्रित अवस्था
इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है।
इस अवस्था के बालक की सभी व्यावहारिक क्रियाएँ अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केन्द्रित रहती हैं।
बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व यानी आत्म-कल्याण से जुड़ा होता है।
परम्पराओं को धारण करने वाली अवस्था
सातवें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारम्भिक काल का सम्बन्ध इस अवस्था से है।
इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है अत: उसमें समाज के बनाए नियमों, परम्पराओं तथा मूल्यों को धारण करने सम्बन्धी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है।
इस अवस्था में उसे अच्छाई-बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुँचेगी।
आधारहीन आत्मचेतना अवस्था
यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है।
इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊँचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है।
यह मेरा आचरण है, मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ इसकी उसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार आचरण और व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है।
पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असन्तुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही असन्तुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है, उसे बदल डालने या परम्पराओं के प्रति विद्रोही रुख अपनाने को उकसाती है।
आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था
नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था है। भली-भाँति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास सम्भव है।
अब यहाँ जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात व्यक्ति विशेष में की जाती है उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच-समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है।
वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धान्त
सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से सम्बन्धित एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त में उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से अन्त:क्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। यदि उसे सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होंगी, तो इसका उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है।
उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरों के हित चिन्तन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता। वह इस आयु में गुड्डे-गुड़ियों, खिलौने, मूर्ति, आदि निर्जीव पदार्थों तथा पशु-पक्षी, मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अन्तर नहीं समझ पाता। शिशु के सामाजिक सम्पर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। अत: सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ-साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारम्भ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग सम्बन्धी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियाँ अपने वय-समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं।
समूह के प्रति उत्पन्न भावना अब केवल टोली या गिरोह विशेष तक ही सीमित है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक सम्पर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। किशोरावस्था में वैयक्तिक विशेषताओं के अतिरिक्त संस्कृति, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यौन सम्बन्धी स्वतन्त्रता और जानकारी इत्यादि उनकी सामाजिक रुचियों और सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करती है।
वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धान्त का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या-समाधान, अर्थात् बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। इसमें वे अपने साथियों के साथ अन्त:क्रिया करते हैं एवं अपने निर्णय पर पहुँचते हैं, शिक्षक का इस कार्य में केवल निर्देश प्राप्त होता है, वह कक्षा पर कठोरता से नियन्त्रण नहीं रखता बल्कि बच्चों को स्वतन्त्रतापूर्वक सोचने एवं समस्या का समाधान करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षक का रवैया केवल सहयोगात्मक एवं निर्देशात्मक होता है।
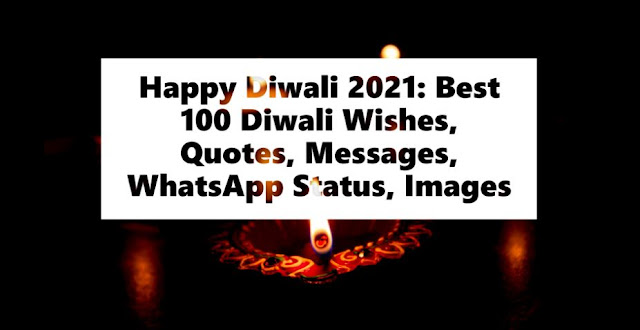
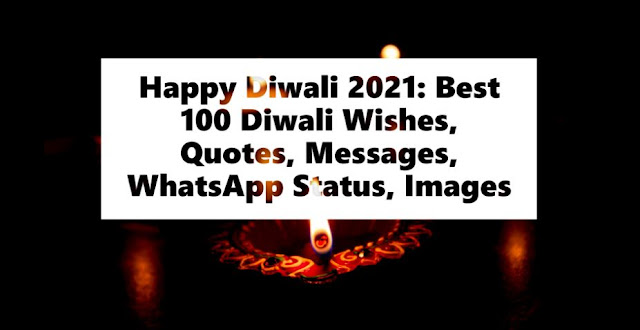
Comments
Post a Comment