3 - अनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव
बाल विकास के अवरोधक
बाल विकास की प्रक्रिया आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है।
वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक इत्यादि बाल विकास को प्रभावित करने वाले आन्तरिक कारक हैं।
सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं वातावरण जन्य अन्य कारक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं।
मानव-व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अन्तःक्रिया का परिणाम होता है।
आनुवंशिकता का स्वरूप तथा अवधारणा
आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी-से-दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम (Heredity) कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी (Genetics) कहा जाता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएँ क्रियाएँ या क्षमताएँ सम्मिलित रहती हैं, जिनको वह अपने माता-पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। आनुवंशिकता जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन (अभिकल्पना) का होना है।
आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। ड संतति में जनक के अधिकतर आधारभूत लक्षण होते हैं। जिन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। आनुवंशिकता का मूलाधार कोष (Cell) है जिस प्रकार एक-एक ईंटों को चुनकर इमारत बनती है ठीक उसी प्रकार से कोषों के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भधारण के समय माँ के अण्डाणु और पिता के शुक्राणु का कोषों में मिलन होता है ताकि एक नये कोष की रचना हो सके। कोषों के केन्द्रक (न्यूक्लियस) के कणों को गुणसूत्र (क्रोमोसोम्स) कहते हैं। गुणसूत्रों का अस्तित्व युग्मों में होता है।
मानव कोष में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 युग्मों में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक युग्म में से एक माँ से आता है और दूसरा पिता से और ये गुणसूत्र आनुवंशिकी सूचना को संचारित करते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र (क्रोमोसोम) में बहुत बड़ी संख्या में जीन्स होते हैं, जोकि शारीरिक लक्षणों के वास्तविक वाहक हैं।
मॉण्टेग्यू और शील फेण्ड के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र में 3000 जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स ही व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं एवं गुणों के निर्धारक होते हैं।
आनुवंशिकता का प्रभाव
शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव
बालक के रंग-रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊँचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। माता के गर्भ में निषेचित युग्मज (जाइगोट) मिलकर क्रोमोसोम्स के विविध संयोजन (कॉम्बीनेशन्स) बनाते हैं। इस प्रकार एक ही माता-पिता के प्रत्येक बच्चे से विभिन्न जीन्स बच्चे में अपने अथवा रक्त सम्बन्धियों के साथ अन्यों से अधिक समानताएँ होती हैं। आनुवंशिक संचारण (ट्रांसमिशन) एक अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है। मनुष्यों में हमें दृष्टिगोचर होने वाले अधिकांश अभिलक्षण, असंख्य जीन्स का संयोजन होता है।
जीन्स के असंख्य प्रतिवर्तन (परम्युटेशन्स) और संयोजन (कॉम्बीनेशन्स) शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अभिलक्षणों में अत्यधिक विभेदों के लिए जिम्मेदार होते हैं। केवल समान अथवा मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में एकसमान सेट के गुणसूत्र (क्रोमोसोम्स) और जीन्स होते हैं क्योंकि वे एक ही युग्मज (सिंगल जाइगोट) के द्विगुणन (डुप्लिकेशन) से बनते हैं। अधिकांश जुड़वाँ भ्रातृवत अथवा द्वि-युग्मक होते हैं जो दो पृथक् युग्मजों से विकसित होते हैं। यह भाइयों जैसे जुड़वाँ भाई और बहनों की तरह मिलते-जुलते होते हैं, परन्तु वे अनेक प्रकार से परस्पर एक-दूसरे से भिन्न भी होते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं।
यदि बालक के माता-पिता गोरे हैं तो उनका बच्चा गोरा ही होगा, किन्तु यदि माता-पिता काले हैं तो उनके बच्चे काले ही होंगे। इसी प्रकार माता-पिता के अन्य गुण भी बच्चे में आनुवंशिक रूप से चले जाते हैं। इसके कारण कोई बच्चा अति प्रतिभाशाली एवं सुन्दर हो सकता है एवं कोई अन्य बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर। जो बालक जन्म से ही दुबले-पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। असन्तुलित शरीर, मोटापा, कम ऊँचाई, शारीरिक असुन्दरता इत्यादि बालक के असामान्य व्यवहार के कारण होते हैं। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुँचती है और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
आनुवंशिकता (वंशानुक्रम) की परिभाषाएँ
जेम्स ड्रेवर "शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता-पिता से सन्तानों में हस्तान्तरण होना आनुवंशिकता है।”
रूथ बैनलेक्ट वंशनुमान माता-पिता से सन्तानों के प्रतिहने वाले ! गुण है।”
पी जिसबर्ट ‘प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविकीय अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता-पिता द्वारा उनकी सन्तानों में हस्तान्तरित करना ही आनुवंशिकता है।”
एच ए पेटरसन एवं बुडवर्थ ‘’ व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएँ प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। है।”
जीव शास्त्रियों के अनुासा ‘’ निषिक्त अण्ड में सम्भावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का योग ही आनुवंशिकता है।”
उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता ; पूर्वजों या माता-पिता द्वारा सन्तानों में होने वाले गुणों का संक्रमण ! है। प्रत्येक प्राणी अपनी जातीय विशेषताओं के आधार पर शारीरिक , मानसिक गुणों का हस्तान्तरण सन्तानों में करते है।
शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन प्रखर अथवा प्रतिगामी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह एक ज्ञात सत्य है कि किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला में रंगों को पहचानने की अन्धता (कलर ब्लाइण्ड नेस) अथवा किन्हीं विशिष्ट रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकती है। एक दादी और माँ, स्वयं रंग-अन्धता से ग्रस्त हुए बिना किसी नर शिशु को यह स्थिति हस्तान्तरित कर सकती है। ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि यह विकृति प्रखर होती है, परन्तु महिलाओं में यह प्रतिगामी (रिसेसिव) होती है।
जीन्स जोड़ों में होते हैं। यदि किसी जोड़े में दोनों जीन प्रखर होंगे तो उस व्यक्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा (जैसे रंगों को पहचानने की अन्धता), यदि एक जीन प्रखर हो और दूसरा प्रतिगामी, तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा।
प्रतिगामी जीन आगे सम्प्रेषित हो जाएगा और यह अगली किसी पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। अत: किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन ही जिम्मेदार होता है। जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं और प्रदर्शित होते हैं, जैसे आँखों का रंग, उन्हें समलक्षणी (फिनोटाइप्स) कहते हैं। ड प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, जब तक कि वे अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते जो अभिलक्षण आनुवंशिक रूप से प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचारित हो जाते हैं परन्तु वे प्रदर्शित नहीं होते
उन्हें समजीनोटाइप (जीनोटाइप) कहते हैं।
बुद्धि पर प्रभाव
बुद्धि को अधिगम (सीखने) की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आपको किस तरह समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है।
गोडार्ड का मत है कि मन्दबुद्धि माता-पिता की सन्तान मन्दबुद्धि और तीव्रबुद्धि माता-पिता की सन्तान तीव्रबुद्धि वाली होती है।
मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है।
बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा सम्बन्धी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईष्र्या एवं वैमनस्यता की भावना अधिक होती है, तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सबका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है।
संवेगात्मक रूप से असन्तुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गम्भीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है।
वातावरण का अर्थ
वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण के मिलने से बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकना। इस प्रकार वातावरण अथवा पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर घेरने वाला। प्राणी या मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है।
वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना ही वातावरण का भी। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है।
वातावरण सम्बन्धी कारक
वातावरण में वे सब तत्व आ जाते हैं, जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरम्भ करने के समय से प्रभावित किया है। गर्भावस्था से लेकर जीवनपर्यन्त तक अनेक प्रकार की घटनाएँ व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके विकास को प्रभावित करती हैं।
गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अन्दर बालक के विकास पर असर पड़ता है बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा न हो, तो उसके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की आशा कैसे की जा सकती है? और यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा न होगा तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है।
जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है, तो उसके विकास की गति सही होगी अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो वह माँ के प्यार के लिए तरसेगा ही। ऐसी स्थिति में उसके सर्वागीण विकास के बारे में कैसे सोचा जा सकता है?
भौतिक परिवर्तन
इसके अन्तर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ आती हैं। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है या जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है । वहाँ मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। ठण्डे प्रदेशों के व्यक्ति सुन्दर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं। धैर्य भी इनमें अधिक होता है। जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं।
सामाजिक कारक
व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन-सहन, परम्पराएँ, धार्मिक कृत्य, रीति-रिवाज, पारस्परिक अन्त:क्रिया और सम्बन्ध आदि बहुत-से तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक एवं बौद्धिक विकास को किसी-न-किसी ढंग से अवश्य प्रभावित करते हैं।
आर्थिक कारक
अर्थ अर्थात् धन से केवल सुविधाएँ ही नहीं प्राप्त होती हैं बल्कि इससे पौष्टिक चीजें भी खरीदी जा सकती हैं, जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। धनहीन व्यक्ति में असुविधा के अभाव में हीन भावना विकसित हो जाती है जो विकास के मार्ग में बाधक है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
सांस्कृतिक कारक
धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। खाने का ढंग, रहन-सहन का ढंग, पूजा-पाठ का ढंग, समारोह मनाने का ढंग, संस्कार का ढंग आदि हमारी संस्कृति हैं। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है उनका विकास ठीक ढंग से होता है लेकिन जहाँ अन्धविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है उस समाज का विकास सम्भव नहीं है।
वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव
शारीरिक अन्तर का प्रभाव
व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किन्तु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगो का शरीर लम्बा एवं गठीला होता है। अनेक पीढ़ीयों से निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग में अन्तर वातावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है।
प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव
कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरण होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। यदि एक महान् व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए, जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध न हो, तो उसका अपने पिता की तरह महान् बनना सम्भव नहीं हो सकता।
व्यक्तित्व पर प्रभाव
व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान् बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आस-पास देखने को मिलते हैं जिनमें निर्धन परिवारों में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएँ प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। न्यूमैन, फ्रीमैन और होलजिंगर ने इस बात को साबित करने के लिए 20 जोड़े जुड़वाँ बच्चों को अलग-अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। उन्होंने एक जोड़े के एक बच्चे को गाँव के फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अन्तर पाया गया। फार्म का बच्चा अशिष्ट, चिन्ताग्रस्त और बुद्धिमान था। उसके विपरीत, नगर का बच्चा, शिष्ट, चिन्तामुक्त और अधिक बुद्धिमान था।
मानसिक विकास पर प्रभाव
गोर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलने पर मानसिक विकास की : गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गन्दा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। अध्ययन में पाया गया कि गन्दे एवं समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल असर पड़ता था|
बालक पर बहुमुखी प्रभाव
वातावरण, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेराम्न का जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक को जन्म के बाद एक भेडिया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ था। कुछ शिकारियों ने उसे 1799 ई. में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 अथवा 12 वर्ष की थी। उसकी आकृति पशुओं-सी हो गई थी। वह उनके समान ही हाथों-पैरों से चलता था। वह कच्चा माँस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सब प्रयास विफल हुए।
आनुवंशिकता एवं वातावरण के बाल विकास पर भावों के शैक्षिक महत्व
विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन-पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। आनुवंशिकता और परिवेश परस्पर इस प्रकार गुंथे हुए हैं कि इन्हें पृथक् करना असम्भव है और बच्चे पर प्रत्येक परस्पर अपना प्रभाव डालता है। इसलिए व्यक्ति के विकास की कुछ सार्वभौमिक विशेषताएँ होती हैं और कुछ निजी विशेषताएँ होती हैं। आनुवंशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी अधिक लाभकारी है कि हम समझे कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है? ताकि बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम सम्भावित विकास के लिए सहायता की जा सके।
हमें साधारणतया यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है या वातावरण? यह प्रश्न पूछना यह पूछने के समान है कि मोटरकार के लिए इंजन अधिक महत्वपूर्ण है या पेट्रोल। जिस प्रकार मोटरकार के लिए इंजन और पेट्रोल का समान महत्च है, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का समान महत्व है। वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है। ये एक-दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी हैं।
बालक को जो मूल प्रवृतियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास वातावरण में होता है, उदाहरण के लिए, यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है, तो उत्तम-से-उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता है। इसी प्रकार बौद्धिक शक्ति वाला बालक प्रतिकूल वातावरण में अपना मानसिक विकास नहीं कर सकता है। वस्तुत: बालक के सम्पूर्ण व्यवहार की सृष्टि, वंशानुक्रम और वातावरण की अन्तःक्रिया द्वारा होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक-दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार आत्मा और शरीर का सम्बन्ध है, उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण का भी सम्बन्ध है। अतः बालक के सम्यक् विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का संयोग अनिवार्य है।
बालक क्या है? वह क्या कर सकता है? उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है? आदि प्रश्नों का उत्तर आनुवंशिकता एवं वातावरण के प्रभावों में निहित है। इनकी जानकारी का प्रयोग कर शिक्षक बालक के सर्वागीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। अत: बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती हैं। बालक को समझकर ही उसे दिशा-निर्देश दिया जा सकता है।
एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बालकों का शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एक जैसा नहीं होता है। शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा है और जिसका मानसिक विकास अच्छा होता है, उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार-प्रकार प्राप्त करता है। वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है, तो उसकी माँसपेशियाँ, हड्डियाँ तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएँ बढ़ती हैं। बौद्धिक क्षमता के लिए सामान्यतः वंशानुक्रम ही जिम्मेदार होता है। इसलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना आवश्यक है।
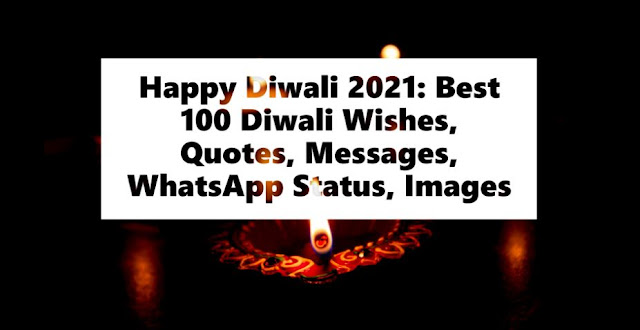
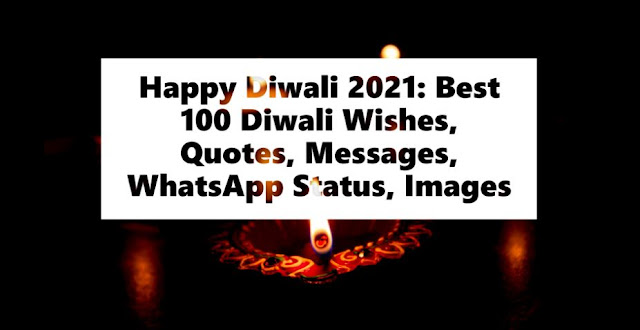
Comments
Post a Comment